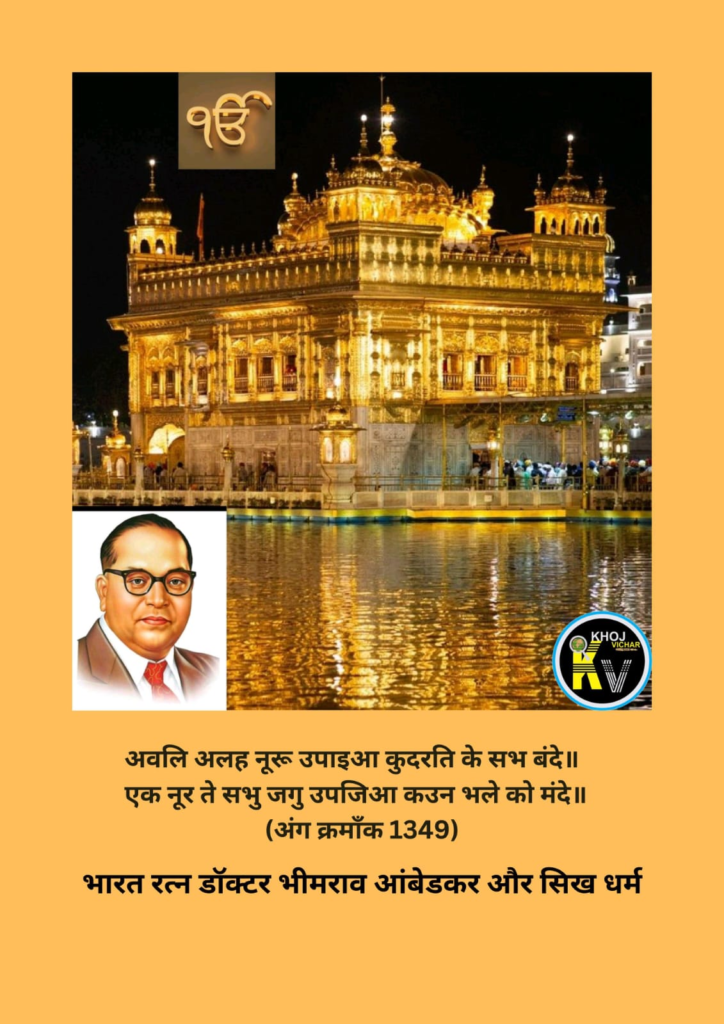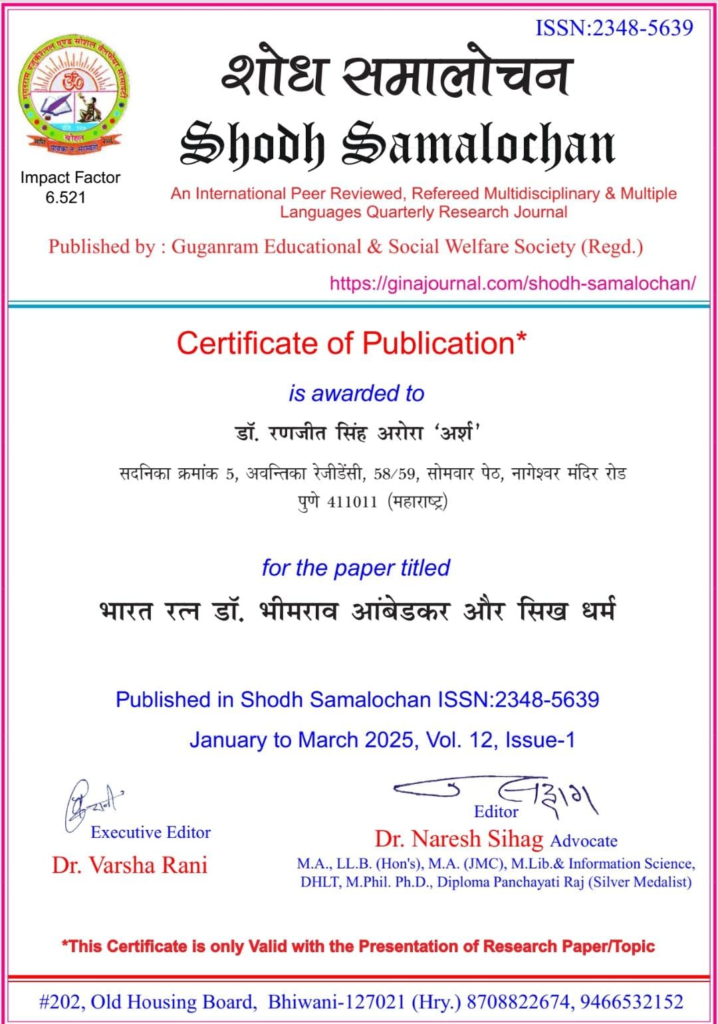भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और सिख धर्म
(एक शोध पूर्ण आलेख / शोध पत्र)
भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर भारत के महानतम समाज सुधारकों, विधिशास्त्र के मर्मज्ञों और संविधान निर्माताओं में अग्रगण्य थे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में छुआछूत, जातिगत भेदभाव तथा सामाजिक असमानता के विरुद्ध निर्भीक संघर्ष किया। वे शिक्षा को मुक्ति का साधन मानते थे और उन्होंने दलित वर्ग को जागरूक कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाया। भारतीय संविधान की रचना द्वारा उन्होंने समानता, न्याय और स्वतंत्रता की मूलभूत नींव रखी। उनके जीवन में मानवता, साहस और विद्वत्ता का अद्वितीय समन्वय था। आज भी उनके विचार करोड़ों जनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारत राष्ट्र उनके योगदान के प्रति सदैव ऋणी रहेगा।
ऐसे युगपुरुष डॉ. आंबेडकर ने सन् 1935-36 में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि वे स्वयं तथा उनके साथ चलने वाले लगभग आठ करोड़ अनुसूचित जातियों (जो भारतीय संविधान में उन जातियों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें पारंपरिक रूप से सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से वंचित माना गया है) के अनुयायी एक स्वर में हिंदू धर्म का परित्याग कर किसी अन्य धर्म को अंगीकार करेंगे। उनके इस निर्णय से भारत के समस्त धार्मिक समुदायों—बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिख आदि—में एक गहन हलचल उत्पन्न हो गई और इन वर्गों के भीतर यह भावना बलवती हुई कि वे इन करोड़ों आत्माओं को अपने-अपने धर्म में सम्मिलित करें।
डॉ. आंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अत्यंत विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और अपने युग के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित एवं प्रतिभा संपन्न विधिवेत्ता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी वकालत की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती थी। यह उनकी आत्मनिर्भरता और असाधारण परिश्रम का प्रतिफल था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे मुंबई के लॉ कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त हुए परंतु उन्होंने अपनी सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित नौकरी का परित्याग कर समर्पित भाव से सामाजिक सुधार के कार्य हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके दलित बंधुओं की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है उन्हें अछूत समझ कर अपमानित किया जाता है। अतः उन्होंने संपूर्ण विश्व के धर्मों का गहन अध्ययन किया, अनेक ग्रंथों और शास्त्रों का मनन किया तथा प्रमुख धर्मगुरुओं और विद्वानों से गंभीर संवाद स्थापित किए।
डॉ. आंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया। जब वे सिख धर्म के सान्निध्य में आए, तो उन्होंने सिखों से एक आत्मीय एवं आदरपूर्ण संबंध स्थापित किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों के नेताओं को स्वयं श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर जाकर माथा टेकने भेजा। वहाँ सभी को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य और संतोष हुआ कि वहां न तो जाति-पाति का कोई भेदभाव है, न कोई रुकावट—सभी को समता का अधिकार प्राप्त है। जब डॉ. आंबेडकर ने अपने सहयोगियों से इस विषय पर चर्चा की, तो भविष्य की कार्यवाही हेतु उन्होंने प्रमुख सिख नेताओं को मुंबई आमंत्रित किया।
सन् 1935 ई. में सिख धर्म के प्रतिनिधियों ने उनसे संवाद स्थापित किया और फिर अनेक बार बैठकें आयोजित की गईं। ‘गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ननकाना साहिब’ की ओर से सरदार नरैण सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जनवरी सन 1936 ई. में मुंबई पहुँचा। इस दल में संत तेजा सिंह, ज्ञानी इंदर सिंह, भाई समुंदर सिंह, सरदार आत्मा सिंह (मुख्य लिपिक, गुरुद्वारा ननकाना साहिब), श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी, तथा मजहबी सिखों में से तीन सेवक शामिल थे।
इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विचारों की पड़ताल करना और उन्हें सिख सिद्धांतों से अवगत कराना था। इस हेतु अंग्रेजी और मराठी में लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर बड़े स्तर पर वितरित की गईं। उन्होंने उन जातियों के प्रमुखों से गहन विमर्श भी किया, जो अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हुआ।
महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों ने पुणे में 11-12 जनवरी 1936 को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु ‘गुरुद्वारा ननकाना साहिब कमेटी’ द्वारा, मुंबई और पुणे की सिंघ सभाओं के सहयोग से, एक भव्य लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने एक समान पंक्तियों में बैठकर भोजन ग्रहण किया। लंगर की सेवा में तथाकथित अनुसूचित जातियों के लोग भी श्रम पूर्वक सम्मिलित हुए। इस आत्मीय आयोजन ने उपस्थित समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला। सम्मेलन में ‘ननकाना साहिब कमेटी’ के कीर्तन जत्थे द्वारा ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी’ की वाणी और विचारों का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण हुआ, जिसे सुनकर जनसमूह भाव विभोर हो उठा।
इसी प्रेरणा से, ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ ने भारत के अन्य प्रांतों में सिख धर्म के प्रचार हेतु 13 अप्रैल सन 1936 ई. को (बैसाखी के पावन अवसर पर) ‘सर्व हिंद सिख मिशन’ की स्थापना की। इसके अंतर्गत अमृतसर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से सिख नेतृत्व तथा अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, विशेष रूप से आमंत्रित भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्वयं सम्मिलित हुए।
इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा हरकिशन सिंह जी का धाराप्रवाह अंग्रेजी भाषण उपस्थित जनों पर अमिट छाप छोड़ गया। इस सम्मेलन एवं उसमें आयोजित समर्पित लंगर ने एक बार फिर सामाजिक समानता के मूल मंत्र को जनमानस में गहराई से अंकित किया।
उस समय तक डॉ. आंबेडकर मुंबई लॉ कॉलेज के प्राचार्य पद से अवकाश ग्रहण कर अपने सार्वजनिक जीवन के नवीन चरण में प्रवेश कर चुके थे। इस सामाजिक नवचेतना के अभियान को गति देने हेतु उन्हें एक समाचार पत्र, एक मुद्रणालय तथा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए एक स्वतंत्र उच्च शिक्षण संस्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने यह प्रस्ताव ‘सर्व हिंद सिख मिशन’ के समक्ष रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया।
उस समय खालसा कॉलेज केवल अमृतसर एवं लायलपुर (अब पाकिस्तान में) स्थित थे। परंतु सिख नेतृत्व की दूरदर्शिता एवं डॉ. आंबेडकर के प्रति श्रद्धा का ही प्रतिफल था कि लगभग दो हजार किलोमीटर दूर मुंबई में एक नवीन कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया।
डॉ. आंबेडकर की प्रेरणा से मिशन ने इस दायित्व का भार हेडमास्टर सरदार केहर सिंह को सौंपा। उस समय ‘सर्व हिंद सिख मिशन’ के पास कोई स्थायी कोष नहीं था, अतः सारा व्यय ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ द्वारा वहन किया गया। भवन निर्माण एवं प्रेस स्थापना हेतु धनराशि की विशेष आवश्यकता थी परंतु आर्थिक सीमाओं के बावजूद सरदार केहर सिंह जी को पाँच हज़ार रुपये के साथ मुंबई भेजा गया।
मुंबई की सिंघ सभा ने सहर्ष सहयोग प्रदान किया तथा पाँच हज़ार रुपये की अतिरिक्त धनराशि को कॉलेज हेतु भूखण्ड के अग्रिम भुगतान के रूप में प्रदान किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, माटुंगा क्षेत्र में इस कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थल का चयन स्वयं डॉ. आंबेडकर ने अपने कर-कमलों से किया। 15 अप्रैल सन 1936 ई. को 27,642 वर्ग गज़ भूमि को ₹6.50 प्रति गज़ की दर से ₹1,79,673 में खरीदकर विधिवत नगर निगम से समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।
डॉ. आंबेडकर की देशव्यापी यात्राओं हेतु भी सरदार केहर सिंह जी द्वारा पाँच हज़ार रुपये और प्रदान किए गए। कुछ ही समय पश्चात डॉ. आंबेडकर विदेश यात्रा से लौटे और जर्मनी की एक शिक्षण संस्था की भवन योजना अपने साथ लाए, जिसे उन्होंने नए कॉलेज की इमारत का मॉडल बनाया।
इस बीच सरदार केहर सिंह तन-मन-धन से भवन निर्माण में संलग्न थे। नियोजित वास्तु शास्त्र स्वरूप के अनुरूप कार्य तीव्र गति से बढ़ा। भवन की रूपरेखा को नगर निगम से स्वीकृति मिल चुकी थी। विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। पुस्तकालय हेतु समुचित पुस्तकें पहुँच चुकी थीं। अब केवल इनका सुनियोजित नियोजन शेष था। इस समस्त कार्य का संचालन डॉ. आंबेडकर स्वयं कर रहे थे।
इन सब उपलब्धियों के बावजूद डॉ. आंबेडकर की ओर से धर्मांतरण की अंतिम घोषणा विलंबित होती जा रही थी। सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर में उनके भेजे छात्र उत्साहपूर्वक अध्ययनरत थे और मुंबई स्थित नवीन कॉलेज के शुभारंभ में भी कोई बाधा नहीं थी। नायगांव में एक अस्थायी भवन में प्रेस स्थापित कर लिया गया था जहाँ से डॉ. आंबेडकर का प्रसिद्ध समाचार पत्र ‘जनता’ नियमित प्रकाशित होने लगा।
इन सबके होते हुए भी डॉ. आंबेडकर किसी अंतिम निर्णय की घोषणा से वंचित रहे। यह मौन कई प्रश्नों को जन्म दे रहा था।
आखिरकार, पंजाब से प्रतिष्ठित सिख प्रतिनिधि—बाबा हरकिशन सिंह, प्रिंसिपल कश्मीरा सिंह, मास्टर सुजान सिंह सरहाली, जत्थेदार तेजा सिंह अकरपुरी तथा सरदार ईश्वर सिंह मझैल—ने दिनांक 23 मई सन 1937 ई. को डॉ. आंबेडकर से विमर्श हेतु महाराष्ट्र के समीप स्थित जंजीरा नामक द्वीप का रुख किया।
मुंबई से सरदार गुरदित्त सिंह सेठी (प्रधान, सिंघ सभा बंबई) और सरदार नरैण सिंह (प्रबंधक) भी इस प्रतिनिधिमंडल से आ जुड़े, और समवेत रूप से यह समस्त दल अगले दिन सायंकाल डॉ. आंबेडकर से भेंट हेतु जंजीरा द्वीप पर पहुँचा। वहाँ एक दीर्घकालिक और गंभीर वार्ता सम्पन्न हुई।
वह समय भारतीय जनमानस में गहन उथल-पुथल का था। सन् 1937 ई. में धर्म परिवर्तन की संभावित लहर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। अनेक संकीर्ण सोच वाले हिंदू नेताओं को यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा था कि डॉ. आंबेडकर का झुकाव सिख धर्म की ओर है। उन्हें भय सताने लगा कि यदि आठ करोड़ दलित वर्ग सिख धर्म को अपनाते हैं, तो इससे हिंदू समाज की जनसंख्या और सत्ता-संतुलन को भारी आघात पहुँच सकता है। यह स्थिति भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक नवीन और शक्तिशाली विचारधारा की स्थापना का संकेत देती थी।
इसी भय के कारण अफवाहें भी तेजी से फैलने लगीं। यह प्रचारित किया गया कि सिखों की एक करोड़ जनसंख्या पर जब आठ करोड़ दलित अनुयायी जुड़ेंगे, तो वे सिख समाज पर हावी हो जाएंगे। किंतु ऐतिहासिक तथ्यों का गहन अध्ययन करने से यह प्रमाणित होता है कि यह केवल मिथ्या प्रचार था। वास्तविकता यह थी कि सिख समाज ने तो अपने दलित भाइयों को सच्चे हृदय से अपनाने का संकल्प किया था।
धर्म परिवर्तन की इस आशंका से भयभीत होकर कुछ हिंदू नेताओं ने षड्यंत्र रचना आरंभ किया। उन्होंने अनुसूचित जाति के कुछ प्रमुख नेताओं को प्रलोभन देकर डॉ. आंबेडकर से पृथक कर दिया और एक ‘हरिजन संस्था’ की स्थापना कर दी। इस योजना को सफल बनाने के लिए हिंदू पूंजीवाद एवं कांग्रेस की सामाजिक प्रतिष्ठा का पूर्णतः उपयोग किया गया। इस प्रचार के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बीच यह भाव प्रबल किया गया कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए।
उसी समय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाश में आया—पश्चिम बंगाल से प्रकाशित पुस्तक Poet and Mahatma, जिसमें महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बीच का पत्राचार संकलित था। 20 सितंबर सन 1936 ई. को महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई ने कविवर टैगोर को गांधी जी की ओर से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि डॉ. आंबेडकर अपने अनुयायियों सहित सिख धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो हिंदू धर्म की जनसंख्या को भारी क्षति पहुंचेगी, जो कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। गांधी जी ने टैगोर से आग्रह किया कि वे डॉ. आंबेडकर को इस निर्णय से रोकें।
इसके प्रत्युत्तर में कविवर टैगोर ने 4 जनवरी सन 1937 ई. को गांधी जी को उत्तर देते हुए लिखा कि उन्होंने अपने पिता के साथ अमृतसर में निवास किया था और वह सिख धर्म की विशेषताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ‘श्री गुरु गोबिंद सिंह जी’ ने जब ‘पंच प्यारे’ सजाए, तब जात-पात के विरुद्ध एक महान क्रांति का सूत्रपात हुआ था। टैगोर ने सिख धर्म को जाति-विहीन समाज का आदर्श बताया और इसे मानव समानता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना। यह पत्राचार आज भी उस युग की धार्मिक चेतना का सजीव प्रमाण है।
अफवाहों का यह चक्र बार-बार इस आशंका को पुष्ट करता रहा कि आठ करोड़ दलित सिख धर्म में सम्मिलित हो कर मूल सिख समाज पर प्रभाव डालेंगे। किंतु सिख कौम ने बारंबार इस तथ्य को खंडित किया और दलित समाज के प्रति अपने स्नेह तथा समरसता को प्रमाणित किया।
इन्हीं घटनाओं के पश्चात डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे में कई बार बैठकें हुईं। इन बैठकों में डॉ. आंबेडकर पर धर्म परिवर्तन का निर्णय स्थगित करने हेतु दवाब डाला गया। एक प्रस्ताव यह भी पारित हुआ कि स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों को तीस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परिस्थिति में दलित समुदाय दो मतों में बँट गया—एक समूह ने इश्तहार प्रकाशित कर हिंदू धर्म में रहने की घोषणा की, जिससे डॉ. आंबेडकर अत्यंत मर्माहत हुए।
इस पृष्ठभूमि में जंजीरा में एक निर्णायक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सिख प्रतिनिधियों—सरदार ईश्वर सिंह, जत्थेदार तेजा सिंह अकरपुरी, मास्टर सुजान सिंह सरहाली, बाबा हरकिशन सिंह और प्रिंसिपल कश्मीरा सिंह जी ने भाग लिया। इस बैठक के उपरांत डॉ. आंबेडकर ने गहरे आत्ममंथन के साथ निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में यदि वे सिख धर्म स्वीकार करते भी हैं, तो उनके साथ केवल मुट्ठी भर लोग ही आ सकेंगे।
डॉ. आंबेडकर के शब्दों में—”मुझे ऐसी हास्यास्पद स्थिति में ला दिया गया है कि यदि मैं अब सिख भी बन जाऊँ, तो मेरा यह क़दम…” (यह वाक्य अधूरा ही रह गया, किंतु इसमें छिपा भाव स्पष्ट था — धर्म परिवर्तन की मूल योजना को अनेक साज़िशों ने बाधित कर दिया)।
डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा—”यदि मैं अब सिख बन भी जाऊँ, तो भी कुछ गिने-चुने लोग ही मेरे साथ आएँगे; इससे हिंदू बहुसंख्यक समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।” इस प्रकार, जंजीरा द्वीप की उस निर्णायक बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित धर्म परिवर्तन, उस समय केवल एक गहन भावनात्मक उद्गार था, जो तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और मानसिक परिस्थितियों के चलते साकार नहीं हो सका।
अगले दिन प्रतिनिधिमंडल जंजीरा से मुंबई लौटा। वहाँ पहुँचकर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ कि क्या 20 जून से कॉलेज को आरंभ किया जाए अथवा नहीं? विचार मंथन की इस प्रक्रिया के दौरान तीन दिवस तक कॉलेज का निर्माण कार्य स्थगित रहा।
अंततः यह सामूहिक निर्णय लिया गया कि अब तक कॉलेज पर लगभग चार लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। भवन लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर था; फर्नीचर, पुस्तकालय हेतु पुस्तक-संग्रह और विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपकरण पहले ही क्रय किए जा चुके थे। मुंबई विश्वविद्यालय से कॉलेज की मान्यता हेतु आवश्यक समस्त पत्राचार भी संपन्न हो चुका था। प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 20 जून सन 1937 ई. से आरंभ होनी प्रस्तावित थी।
ऐसे में, यदि इस समय कॉलेज की स्थापना को स्थगित कर दिया जाता अथवा परित्याग कर दिया जाता, तो यह न केवल एक गंभीर त्रुटि होती, बल्कि सिख समुदाय की प्रतिष्ठा पर भी गहन आघात पहुंचता। इससे न केवल मुंबई में सिखों की सामाजिक छवि पर प्रश्नचिह्न लगता, अपितु यह एक ऐसा दाग होता, जिसे शीघ्र धो पाना अत्यंत कठिन होता। अतः समस्त प्रतिनिधियों की सामूहिक सहमति से, ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ से अनुमति प्राप्त कर, कॉलेज को नियत समय पर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व का भार श्री गुरु सिंघ सभा, मुंबई के तत्कालीन प्रधान सरदार गुरदित्त सिंह जी को सौंपा गया, जबकि पूर्व निर्धारित रूप से प्रिंसिपल नियुक्त कश्मीरा सिंह जी को समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक तैयारियाँ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
तीन दिवस की अस्थायी रुकावट के पश्चात, पुनः तीव्र गति से कॉलेज निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया। पंजाब से पधारे प्रतिनिधि अपने-अपने नगरों की ओर लौट गए। खालसा कॉलेज, मुंबई की भव्य त्रि-मंजिला इमारत, जिसमें कुल चालीस कक्ष, दोनों ओर खुले एवं सौंदर्य युक्त बरामदे, तथा ऊपर की मंज़िल पर 50×54 फुट का विशाल गुरुद्वारा साहिब का हॉल निर्मित किया गया।
कॉलेज के प्रारंभिक काल में कुछ चुनौतियाँ अवश्य उत्पन्न हुईं, किंतु ‘गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ननकाना साहिब’ द्वारा समयोचित सहयोग से उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब कॉलेज की बिक्री पर विचार हुआ, परंतु सभी सदस्यों के दृढ़ विरोध के कारण यह प्रस्ताव तिरस्कृत कर दिया गया।
यह वही गौरवशाली संस्था है जो डॉक्टर आंबेडकर के सुझाव, दूरदृष्टि और सामाजिक चिंतन की प्रत्यक्ष परिणति है। आज यह संस्थान महाराष्ट्र की अग्रणी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष स्थान रखता है और सिख पंथ की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सेवाएँ दे रहा है। यह संस्था डॉ. आंबेडकर और सिख समाज के पारस्परिक प्रेम, सहयोग तथा सांझे उद्देश्यों की साक्षी है। वर्तमान समय में यह कॉलेज शैक्षणिक सेवाओं के साथ-साथ न्यूनतम शुल्क में मुंबई वासियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएँ भी प्रदान कर रहा है।
जब देश स्वतंत्र हुआ, तब डॉक्टर आंबेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा गया। उन्होंने संविधान का निर्माण कर राष्ट्र को न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता का सूत्र प्रदान किया। किंतु, जब उन्होंने अपने अनुयायियों सहित सिख धर्म में दीक्षित नहीं होने का निर्णय लिया, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह के माध्यम से बौद्ध धर्म (बोध धर्म) का अंगीकार किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग पांच लाख अनुयायियों सहित विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह आयोजन दीक्षाभूमि, नागपुर में संपन्न हुआ, जो आज एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है।
डॉ. आंबेडकर का यह निर्णय जातिवाद, अस्पृश्यता एवं सामाजिक विषमता के विरुद्ध एक ऐतिहासिक क्रांति के रूप में इतिहास में अंकित है। उन्होंने कहा था—”मैं हिन्दू धर्म में जन्मा, यह मेरे वश में नहीं था; परंतु मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा।”
सिख धर्म के साथ डॉ. आंबेडकर का सजीव संबंध प्रारंभ से लेकर जीवन की अंतिम वेला तक बना रहा। जब भी हम सिख साहित्य का गहन अध्ययन करते हैं, तो किसी न किसी संदर्भ में डॉ. आंबेडकर की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय संसद में उनके संबंध सिख सांसदों से भी अत्यंत आत्मीय एवं भ्रातृ भावनाओं से परिपूर्ण रहे। दुर्भाग्य से, बस्स. . . . . कुछ संयोग न बन सके।
सिख धर्म एवं गुरबाणी में जात-पात और ऊँच-नीच का कोई स्थान नहीं है। ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी’ में संत रविदास, संत नामदेव तथा अन्य महान संतों की वाणी संकलित है, जिन्हें सिख पंथ में वही सम्मान प्राप्त है जो स्वयं सिख गुरुओं को है। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी हमारे दलित भाई इस आत्मिक संबंध को ससम्मान स्वीकारते हुए सिख पंथ से गहरा स्नेह रखते हैं कारण गुरुवाणी का फरमान है-
अवलि अलह नूरू उपाइआ कुदरति के सभ बंदे॥
एक नूर ते सभु जगु उपजिआ कउन भले को मंदे॥
(अंग क्रमाँक 1349)
अर्थात, समस्त सृष्टि एक ही ईश्वर के प्रकाश से उत्पन्न हुई है, फिर कौन श्रेष्ठ और कौन निम्न?
साभार — उपरोक्त शोध पूर्ण आलेख के स्त्रोत: ‘गुरु पंथ खालसा’ के प्रतिष्ठित पत्रकार सरदार हरजिंदर सिंह जी रंधावा (पंजाब टेलीविज़न फ्रेम) द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह जी से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित एवं ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर’ द्वारा प्रकाशित मासिक ‘गुरमत प्रकाश’ के मार्च अंक में गुरुमुखी में प्रकाशित आलेख गाथा: खालसा कॉलेज बंबई (लेखक: सरदार हरविंदर सिंह जी) के सौजन्य से।
नोट:-1. ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी’ के पृष्ठों को गुरुमुखी में सम्मान पूर्वक अंग कहकर संबोधित किया जाता है। लेख में प्रकाशित चित्र काल्पनिक है।
2. गुरबाणी का हिंदी अनुवाद गुरबाणी सर्चर एप को मानक मानकर किया गया है।
साभार– लेख में प्रकाशित गुरुवाणी के पद्यों की जानकारी और विश्लेषण सरदार गुरदयाल सिंह जी (खोज-विचार टीम के प्रमुख सेवादार) के द्वारा प्राप्त की गई है।
विशेष नोट- उपरोक्त आलेख “भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर और सिख धर्म” को अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल ‘शोध समालोचन’ (ISSN: 2348-5639) के जनवरी-मार्च 2025, खंड 12, अंक 1 में स्थान प्राप्त हुआ है। इस उत्कृष्ट शोध-कार्य के लिए डॉ. ‘अर्श’ को ‘शोध समालोचन’ संस्था की ओर से “Girdhari Lal Ghasi Ram Sihag Research Excellence Award” से सम्मानित किया गया है।