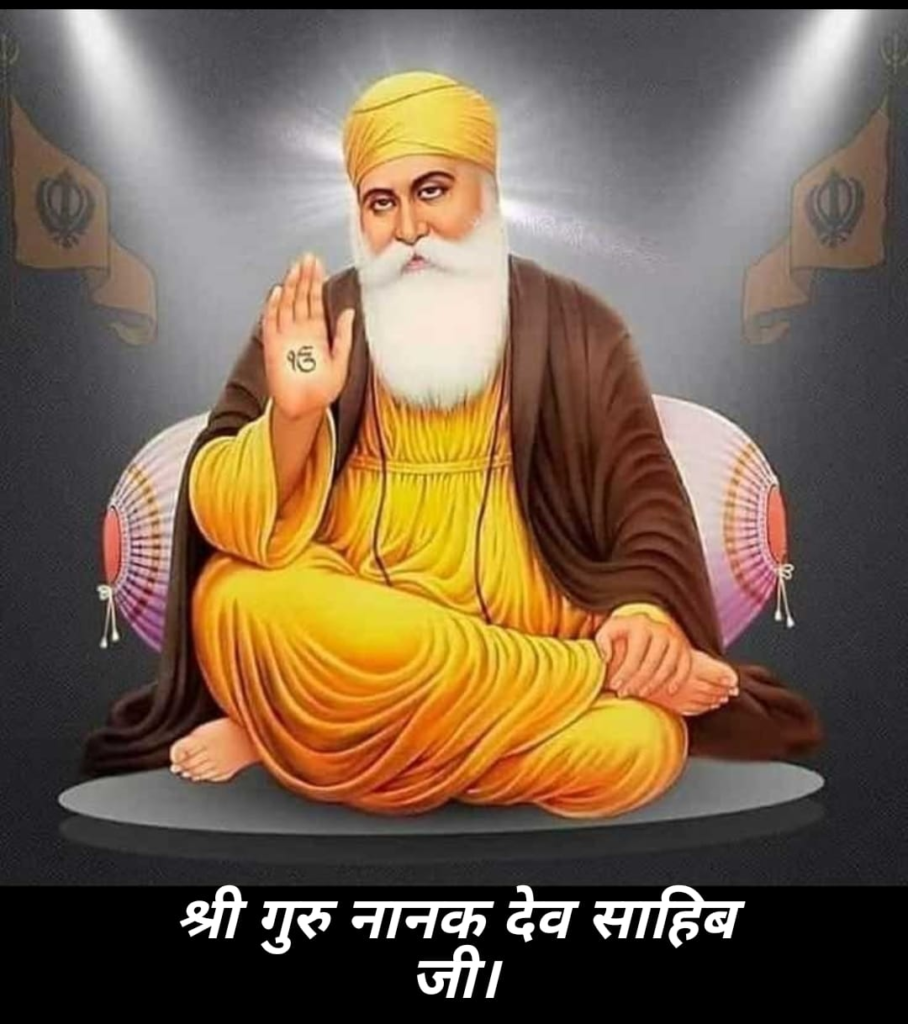श्री गुरु नानक देव साहिब जी और उनकी चार उदासी यात्राएँ
सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव साहिब जी द्वारा उनके जीवन काल में की गई चार उदासी यात्राओं का महान महत्व है। ‘उदासी’ शब्द का अर्थ है उपरामता या वैराग्य, जो सांसारिक सुख, भौतिक संसाधन, परिवार और मोह-ममता के त्याग का प्रतीक है। गुरमत के अनुसार, उदासी का तात्पर्य है कि एक जिज्ञासु अपने आप को मोह-माया और व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त कर, देश-विदेश की यात्राएँ केवल किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करे। इस प्रकार की यात्रा ही उदासी यात्रा कहलाती है। वास्तव में, उदासी फकीरी का वह मार्ग है जिस पर चलने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को संयमित कर भूख-प्यास, असहज मौसम और अनेक प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इन यात्राओं के दौरान गुरु साहिब जी जहाँ भी गए, उन्होंने वहाँ के लोगों की भाषा, बोली, और वेशभूषा को अपनाते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उस समय के सिद्धों, योगियों और संतों ने उनकी वेशभूषा और शैली को देख कर प्रश्न किए, जिनका वर्णन गुरबाणी में इस प्रकार मिलता है-
“कवन तुमे किआ नाउ तुमारा कउनु मारगु कउनु सआओ।
साचु कहउ अरदासि हमारी हउ संत जना बलि जाओ।
कह बैसहु कह रहीऐ वाले कह आवहु कह जाओ।
नानकु बोलै सुणि बैरागी किआ तुमारा राहो।”
(अंग क्रमांक 938)
सिद्धों ने गुरु साहिब से प्रश्न किया कि “तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा कौन-सा मार्ग है? और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है?” गुरु साहब का उत्तर भी गुरबाणी में इसी प्रकार अंकित है –
“गुरमुखि खोजत भए उदासी।
दरसन कै ताई भेख निवासी।
साच वखर के हम वणजारे।
नानक गुरमुखि उतरसि पारे।”
(अंग क्रमांक 939)
गुरु साहिब ने स्पष्ट किया कि वह उन गुरु भक्तों की खोज में निकले हैं जो ‘गुरु मंत्र’ का जाप करते हैं। उनके अनुसार, ‘सच के व्यापारी’ ही गुरु कृपा से इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु साहब की यह उदासी यात्राएँ केवल पर्यटन नहीं थीं; इनका उद्देश्य था समाज को सत्य का मार्ग दिखाना।
उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। समाज में अंधविश्वास, कर्मकांड, जात-पात और ऊँच-नीच का भेदभाव व्याप्त था। हिंदू समाज में वर्ण-व्यवस्था के कठोर विभाजन ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में समाज को बाँट दिया था, जिससे ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और जातीय भेदभाव बढ़ गया था। नारी जाति को निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें सम्मान का अधिकार नहीं दिया जाता था। मुस्लिम हुक्मरानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे और हिंदू स्त्रियों की सुरक्षा सदैव खतरे में रहती थी। पंडित, काजी और जोगी, धर्म के ठेकेदारों ने समाज को भ्रमित कर अपने स्वार्थ साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने अपनी चार उदासी यात्राओं के माध्यम से समाज को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।
गुरु साहिब जी की यह उदासी यात्राएँ वास्तव में उस युग की दिग्विजय यात्राएँ थीं, जिनमें उन्होंने लगभग 36,000 मील की दूरी तय की। इस आलेख में उनके द्वारा की गई इन चार उदासी यात्राओं का संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। निश्चित ही ये उदासी यात्राएँ मात्र देशाटन नहीं थीं, बल्कि मानवता को अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करने का एक दिव्य प्रयास थीं।
पहली उदासी पूर्व की ओर : (30 अगस्त सन 1497 ई. से 24 अक्टूबर सन 1509 ई. तक)
श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने अपनी पहली यात्रा, जिसे प्रथम उदासी के नाम से जाना जाता है, 30 अगस्त सन 1497 ई. (संवत् 1554, 01 अस्सु) को अपने साथी रबाबी भाई मरदाना के साथ सुल्तानपुर से प्रारंभ की। यह यात्रा महज भौगोलिक परिधि तक सीमित नहीं थी; यह एक आत्मिक यात्रा थी, जिसका उद्देश्य मानवता को आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करना था। सुल्तानपुर से प्रस्थान कर गुरु जी ने लाहौर, कंगनपुर, रोशन भीला, और तलवंडी जैसे विभिन्न स्थानों पर अपनी दिव्य शिक्षाओं का प्रचार किया।
तलवंडी से गुरु साहिब सैयदपुर, सरसा, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, और कोटद्वार जैसे पवित्र स्थलों पर गए, जहाँ उन्होंने लोगों को अपने उपदेशों से संतृप्त किया। अल्मोड़ा, नानकमत्ता, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस और पटना होते हुए वे गया (बिहार) पहुँचे। बिहार में गया से लेकर हज़ारीबाग, रांची, चाईबासा और केंदुझार जैसे स्थानों पर उनके प्रवचन और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला।
इसके बाद गुरु जी ने उड़िसा की ओर यात्रा की और भुवनेश्वर होते हुए पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। वहाँ से गुरु जी केंद्रपाड़ा, बालासोर, बेलदा, खड़गपुर, हावड़ा, कोलकाता और फरीदपुर होते हुए ढाका पहुँचे। ढाका से चाँदपुर और सप्तद्वीप संघ समूह के क्षेत्रों में सतिनाम का प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों को आत्मिक जीवन की राह दिखाई।
आगे बढ़ते हुए गुरु साहिब ने अगरतला, अंबासा, मानु, कुमारघाट और करीमगंज का रुख किया। इंफाल, विष्णुपुर और चंदेल होते हुए उन्होंने बर्मा की यात्रा की। बर्मा में भी उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों का हृदय प्रभावित किया और उन्हें सच्चे मार्ग की प्रेरणा दी। बर्मा से लौटकर चंदेल, उखरुल, कोहिमा, दीमापुर, गोलाघाट, नौगांव और गुवाहाटी होते हुए गुरु जी भूटान की पुरानी राजधानी पारो पहुँचे।
पारो से गुरु जी गंगटोक (सिक्किम) और चुंगथांग होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुँचे। वहाँ से तिब्बत की ओर पैदल यात्रा कर उन्होंने ल्हासा में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश फैलाया। तिब्बत से आगे गुरु जी चीन के शंघाई बंदरगाह पहुंचे, जहाँ उन्होंने नानकिंग और नानकिंआंग जैसे शहरों में प्रवास कर अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया। पाँच वर्षों तक चीन में रहकर उन्होंने असंख्य लोगों की आत्मिक और मानसिक शंकाओं का समाधान किया और उन्हें सुमिरन का मार्ग दिखाया। चीन से लौटकर गुरु जी पुनः ल्हासा, काठमांडू, बिरगनी, मोतिहारी, गोरखपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में संक्षिप्त ठहराव के बाद, उन्होंने पानीपत, करनाल, सुनाम और संगरुर का मार्ग अपनाते हुए लगभग 12 वर्षों की इस दिव्य यात्रा को 24 अक्टूबर 1509 ई. को सुल्तानपुर में समाप्त किया।
यह यात्रा मात्र स्थलों का भौगोलिक अवलोकन नहीं थी; यह सत्य की खोज और सत्य के प्रचार-प्रसार की महान यात्रा थी, जिसने समाज को धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव से मुक्त कराने की दिशा में एक अनमोल योगदान दिया। गुरु साहिब की प्रथम उदासी ने भारतवर्ष में एक नई आध्यात्मिक चेतना का संचार किया, जो उनके अनन्य प्रेम, समर्पण और त्याग का जीवंत प्रमाण है।
दूसरी उदासी: दक्षिण की ओर (20 मार्च सन 1510 ई. से 25 मार्च सन 1515 ई. तक)
श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने अपनी दूसरी उदासी की यात्रा 20 मार्च सन 1510 ई. में आरंभ की, जिसमें उनके साथ भाई बाला, भाई मरदाना, भाई सैदो और भाई सींहो जैसे चार समर्पित अनुयायी थे। भाई मरदाना और भाई बाला जी गुरु जी की वाणी को रागों में बाँधकर गायन करते, जबकि भाई सैदो और भाई सींहो सतिगुरु के मुखारविंद से उच्चारित वाणी को कलमबद्ध करने का कार्य करते थे।
गुरु जी ने इस उदासी की शुरुआत सुल्तानपुर से की और लाहौर, तलवंडी, दीपालपुर, पाकपटन, और सरसा होते हुए बीकानेर पहुँचे। यहाँ से गुरु जी जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरे। अजमेर में, जहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, गुरु जी ने स्थानीय संतों और विद्वानों से विचारों का आदान-प्रदान किया। पुष्कर में, गुरु-घाट, पंचकुंड, संतपुरा और ब्रह्मपुरा पर पंडितों और जोगियों से संवाद कर गुरु जी ने सत्य का सन्देश प्रसारित किया।
इसके पश्चात गुरु साहिब चित्तौड़गढ़, उदयपुर और माउंट आबू की ओर बढ़े, जहाँ जैनी साधुओं को उन्होंने आंतरिक और बाह्य शुद्धि का मार्ग बताते हुए एकमात्र प्रभु परमात्मा का सुमिरन करने की प्रेरणा दी। वहाँ से वे पालनपुर, लखपत, भुज, मांडवी, नवलखी, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर होते हुए जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ के बाद सोमनाथ, पालीताणा, भावनगर, साबरमती, बड़ौदा और सूरत तक यात्रा की। फिर नासिक, ठाणे, पुणे, बारसी, पंढरपुर, सांगली, कोल्हापुर और गोवा पहुँचे। गोवा से गुरु जी ने बेंगलुरू, माँडिया, मैसूर, कोझीकोड, कोयंबटूर, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम और पल्लिपुरम होते हुए मदुरै तक की यात्रा की। वहाँ गुरु जी ने स्थानीय पंडितों, सिद्धों, जोगियों और सन्यासियों से ज्ञान-गोष्ठी कर उन्हें ईश्वर के सच्चे मार्ग का सन्देश दिया। अगले चरण में गुरु जी कन्याकुमारी पहुँचे और वहाँ से समुद्री यात्रा करते हुए श्रीलंका के कोलंबो नगर पहुँचे।
श्रीलंका में श्री गुरु नानक देव जी का प्रवास
श्रीलंका में गुरु जी ने कोलंबो से कैंडी, नुवारा एलीया, कत्तरगामा, बाटीकलोआ, त्रिंकोमाली, अनुराधापुरा और जाफना जैसे स्थानों का भ्रमण किया। जाफना के आसपास के मंदिरों जैसे कांदास्वामी कोविल, नागर कोविल, वस्सीपुरम और अमल कोविल में जाकर गुरु जी ने आध्यात्मिक उपदेश दिए। इस दौरान वे श्रीलंका में लगभग एक वर्ष रहे और लगभग चौदह सौ गांवों का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका निवारण किया। श्रीलंका की जनता ने गुरु जी को ‘नानक बुद्ध’ के रूप में मान्यता दी और उनका अपार आदर सत्कार किया।
श्रीलंका से वापसी यात्रा
गुरु जी श्रीलंका से वापस भारत लौटते हुए तालेमन्नार, धानुषकोडी और रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम में अल्पकालिक प्रवास के बाद वे रामनाथपुरम, मदुरै और नागापट्टिनम होते हुए समुद्री मार्ग से जकार्ता (जावा, इंडोनेशिया) पहुँचे। वहाँ से सिंगापुर और मलेशिया में भ्रमण कर लोगों को प्रभु के नाम से जुड़ने का संदेश दिया और मलेशिया से वापस नागापट्टिनम बंदरगाह लौटे। नागापट्टिनम से कुंभकोणम की ओर बढ़े और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन कर लोगों में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया।
गुरु जी की यह दक्षिण उदासी न केवल एक यात्रा थी, बल्कि एक दैवीय अभियान था जिसने जनमानस को धार्मिक कट्टरता और भौतिक सुखों के मोह से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनका हर पड़ाव एक संदेश था, और उनका हर उपदेश उस समय के समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का एक प्रयास था।
तीसरी उदासी: उत्तर की ओर (24 जून सन 1515 ई. से 20 सितंबर सन 1517 ई. तक)
लगभग तीन महीने सुल्तानपुर में रुकने के पश्चात, श्री गुरु नानक देव जी ने 24 जून सन 1515 ई. को अपनी तीसरी उदासी के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा में उनके साथ उनके अनन्य सहयोगी भाई मरदाना और भाई बाला भी थे। इस बार गुरु जी ने सुल्तानपुर से गुरदासपुर, पठानकोट, चंबा और कांगड़ा होते हुए प्रसिद्ध ज्वाला जी मंदिर की ओर यात्रा की। ज्वाला जी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ निरंतर पाँच अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित रहती हैं। यहाँ गुरु जी की भेंट अर्जुन नामक एक नंगे तपस्वी से हुई। गुरु जी ने उन्हें वैराग्य और तपस्या के बाहरी आडंबरों को छोड़कर गृहस्थ जीवन में रहकर परम पद प्राप्त करने की राह दिखाई। तपस्वी अर्जुन गुरु जी के उपदेश से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने और नाम सुमिरन की राह पर चल पड़े।
ज्वालामुखी से गुरुजी मनाली और कुल्लू घाटी होते हुए मणिकरण पहुँचे, जहाँ गंधक के गर्म पानी के चश्मे प्रसिद्ध हैं। मणिकर्ण से वे मंडी और रावलसर पहुँचे। यहाँ स्थित झील के किनारे कई मंदिर हैं, जिनमें लोमा ऋषि, शंकर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर प्रमुख हैं। रावलसर से गुरु जी मंडी लौटे और फिर बिलासपुर होते हुए कीरतपुर पहुँचे।
कीरतपुर में गुरु जी की भेंट सूफी फकीर बुढण शाह से हुई, जो एक पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने गुरु जी को बकरियों का दूध भेंट किया, किंतु गुरु जी ने विनम्रता से उस समय इसे ग्रहण करने से इनकार किया। इस पर फकीर बुढणशाह ने अपनी श्रद्धा में दूध को धरती में सुरक्षित रख दिया और संकल्प लिया कि वह दूध उस दिन की प्रतीक्षा करेगा जब गुरु जी इसे ग्रहण करेंगे। यह भविष्यवाणी वर्षों बाद सच हुई जब श्री गुरु नानक देव साहिब के रूप में साहिबजादा बाबा गुरुदत्ता जी ने उस दूध का सेवन किया और बुढणशाह की श्रद्धा का मान रखा।
कीरतपुर से आगे, गुरु जी नालागढ़, पिंजौर, जौहडसर और माहीसर होते हुए शिमला पहुँचे। जौहडसर में गुरु जी ने बलि प्रथा और अन्य अनिष्टकारी प्रथाओं से लोगों को विमुक्त कर परमपिता की सच्ची उपासना की प्रेरणा दी। माहीसर में उन्होंने पर्वत पर छड़ी लगाकर मीठे जल का स्रोत उत्पन्न किया, जो माहीसर तालाब के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
शिमला से आगे की यात्रा में गुरु जी कालपा, पूह, नाको और कौरिक होते हुए शिपीका ला दर्रा पार कर लाहौल और स्पीति की बर्फानी घाटियों में पहुँचे। वहाँ से थागा ला दर्रा पार कर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड, कैलाश पर्वत और सुमेर पर्वत का भ्रमण किया। मानसरोवर से लौटते समय उन्होंने बशहर किन्नौर के रास्ते तिब्बत में यात्रा की, जहाँ वे जम्बू और ज्ञार्सा नामक तिब्बती नगर पहुँचे।
तिब्बत से लौटते हुए गुरु जी ने लेह, पत्थर साहिब और खलसी होते हुए कारगिल का रुख किया। कारगिल से दराज, बांदीपुरा और वूलर झील के किनारे होते हुए बारामुला पहुँचे। बारामुला से श्रीनगर की यात्रा में, गुरु जी ने शंकराचार्य मंदिर के निकट कई दिनों तक पंडितों, साधु-सन्यासियों और विद्वानों के साथ विचार गोष्ठियां की। वहाँ से गुरु जी हरमुख गंगा और सोनमर्ग होते हुए अमरनाथ पहुंचे, जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हुए मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति की प्रेरणा दी। अमरनाथ से लौटते हुए गुरु जी पहलगांव, मटन, और अन्य पवित्र स्थलों पर भी गए। इस तीसरी उदासी ने लोगों को बाह्य आडंबरों से मुक्त कर आध्यात्मिकता के शाश्वत मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
चौथी उदासी: पश्चिम की ओर (27 मार्च सन 1518 ई. से 30 दिसंबर सन 1521 ई. तक)
श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पूर्व, दक्षिण और उत्तर की उदासी यात्राओं को सफलतापूर्वक पूर्वक कर लिया था। इन यात्राओं का उद्देश्य था – “न को हिन्दू, न मुसलमान” के सिद्धांत को स्थापित करना और संसार में फैले कर्मकांडों, भेदभाव, जात-पात और आडंबरों से लोगों को मुक्त कर परमात्मा के नाम से जोड़ना। गुरु जी ने लोगों को किरत करने (ईमानदारी से मेहनत करना), वंड छकना (बांटकर खाना) और नाम जपना (प्रभु स्मरण करना) सिखाया। समाज में समरसता, नारी सम्मान और भाईचारे का संदेश देकर उन्होंने हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की ज्योति का संचार किया। अब गुरु जी का मन इस्लामी देशों के लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने के लिए प्रेरित हुआ।
तीसरी उदासी के बाद गुरु जी सुल्तानपुर लौट आए थे। अपनी चौथी यात्रा की शुरुआत से पहले गुरु जी पखोके गाँव (नैरोवाल) में अपने रबाबी साथी भाई मरदाना के साथ अपने परिवार और बच्चों को अपने अनन्य शिष्य भाई अजित्ता को सौंपकर माता-पिता से मिलने तलवंडी पहुंचे। माता त्रिप्ता जी की तबीयत खराब थी, और उनके पास कुछ दिन रहकर गुरु जी ने उनकी सेवा की। परंतु प्रभु का विधान कुछ और ही था; 15 मार्च 1518 ई. को माता त्रिप्ता जी इस संसार से विदा हो गईं। माता के देहांत के तीन दिन पश्चात् ही पिता मेहता कालू जी भी परलोक सिधार गए। माता-पिता के देहांत के पश्चात्, गुरु जी ने घर का सारा सामान गरीबों में बांट दिया, जमीन चाचा लालचंद को सौंप दी और प्रभु की इच्छा मानते हुए 27 मार्च 1518 ई. को एक हाजी का वेश धारण कर, नीले वस्त्र पहनकर अपनी चौथी और सबसे लंबी यात्रा पर निकल पड़े। भाई गुरदास जी ने इस क्षण को अपनी वाणी में यूं चित्रित किया है:
“नील वस्त्र ले कपड़े पहिरे तुरक पठाणी अमलु कीआ”
गुरु जी ने तलवंडी से लाहौर, लाहौर से पाकपटन, तुलंमा, मखदूमपुर और मुल्तान का मार्ग अपनाया। मुल्तान से उच्च शरीफ, फिर शिकारपुर (सिंध), और ठट्टा होते हुए लासबेला (बलूचिस्तान) पहुँचे। यहाँ से कराची और फिर शक्तिपीठ हिंगलाज माता के दर्शन के लिए गए। हिंगलाज में पूजन उपरांत गुरु जी सोन मयानी बंदरगाह पहुँचे, जहाँ से समुद्री जहाज द्वारा वे सऊदी अरब के जैद्दा पहुँचे। जैद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से बगदाद होते हुए जॉर्डन और फिर मिश्र (काहिरा) पहुँचे। मिश्र से साउथ अफ्रीका होते हुए युगांडा पहुँचे और वहाँ से सीरिया की ओर बढ़े। सीरिया से तुर्की, तुर्की से इस्तांबुल होते हुए आज़रबाइजान (रूस) और फिर सुराखानी मंदिर तक की यात्रा की, जहां गुरु जी ने लोगों को आत्मिक मार्ग दिखाया। ईरान में, गुरु जी का मिलन सूफी फकीर शिराज से हुआ। शिराज ने अदब के साथ गुरु जी का स्वागत किया, किंतु अपने मन में थोड़ा गर्व भी महसूस किया और गुरु जी को एक मूल्यवान हीरा भेंट किया। गुरु जी ने संत की मानसिक स्थिति को भांपते हुए, भेंट को पर्वत पर फेंक दिया। देखते ही देखते वह पर्वत हीरों का पर्वत बन गया। संत का घमंड चूर हुआ और वह आत्मिकता की सच्ची समझ को प्राप्त कर सका। ईरान से गुरु जी तबरेज़, इस्फ़हान और तुर्किस्तान होते हुए उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर पहुँचे, फिर ताशकंद और वहाँ से कंधार और काबुल की ओर बढ़े। काबुल से गुरु जी फरहा, जलालाबाद, और हजारा होते हुए पेशावर पहुँचे। हसन अबदाल में कुछ समय प्रवास कर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श किया। यहाँ से सियालकोट और सैदपुर ऐमनाबाद पहुँचे। ऐमनाबाद में बाबर के हमले के कारण गुरु जी को कुछ समय रुकना पड़ा। अपनी इस चौथी और अंतिम उदासी को संपन्न करते हुए 30 दिसंबर सन सन 1521 ई. को गुरु नानक देव जी अपने नए बसाए गाँव करतारपुर लौट आए। भाई गुरदास जी ने करतारपुर में गुरु जी के आगमन का अपनी वाणी में इस प्रकार चित्रण किया:
“फिरि बाबा आया करतारपुरि, भेखु उदासी सगल उतारा।
पहिरि संसारी कपड़े मंजी बैठि कीआ अवतारा।”
इस चौथी उदासी के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने मानवता को एकता, प्रेम और सच्चे धर्म की शिक्षा दी, जिसे आज भी मानवता का अमूल्य संदेश माना जाता है।
निश्चित ही इन दिग्विजय उदासी यात्राओं के माध्यम से गुरु साहिब ने पैदल यात्रा करते हुए विश्व कल्याण हेतु जन उपदेश देकर लाखों लोगों का उद्धार किया| ‘सतिनाम’ का प्रचार करते हुए प्रभु के सिमरन की दात बक्शी| आम लोगों को केवल एक ही परमपिता-परमेश्वर की पूजा आराधना करने की प्रेरणा दी|